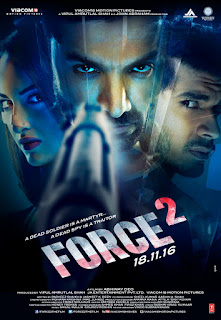संजय गुप्ता की ‘काबिल’
देखते वक़्त अक्सर मिथुन चक्रवर्ती और उनकी कुछ बहुत बेहतरीन फिल्मों की याद
बरबस आ जाती है. लगता है, जैसे अभी भी मिथुन दा का ज़माना पूरी तरह गया
नहीं. ‘आदमी’, ‘जनता की अदालत’, ‘फूल और अंगार’ जैसी फिल्मों
को परदे पर धूम मचाते देखते हुए अभी गिन-चुन के सिर्फ 24-25 साल ही तो गुजरे हैं.
भ्रष्ट राजनेताओं और उनके तलवे चाटते पुलिस महकमे से तमाम जुल्म-ओ-सितम का बदला
लेने के लिए जब मिथुन दा कमर कस के खड़े होते थे, अचानक जैसे बलात्कार की
शिकार उनकी बहन अपनी बहन लगने लगती थी, और अर्जुन, गुलशन ग्रोवर, हरीश पटेल जैसे
गुंडे अपने ही जानी दुश्मन. सिनेमा की ताक़त ही यही होती है. पर सवाल सिर्फ इतना है
कि अगर उन तमाम फिल्मों को घोर लोकप्रियता के बावजूद आज हम ‘बी-ग्रेड सिनेमा’ की श्रेणी
में रखते हैं, तो ‘काबिल’ को भी इस काबिल क्यूँ नहीं समझा जाना चाहिए? या
फिर शायद हमें इसके लिये 24-25 साल और इंतज़ार करना होगा.
संजय गुप्ता कोरियाई फिल्मों के
मुरीद रहे हैं. गाहे-बगाहे कभी चुरा कर, तो कभी 56 इंची सीने के साथ रीमेक अधिकार
खरीद कर उन्हीं फिल्मों को हिंदी में ज्यों का त्यों परोसते रहे हैं. ऐसे में विजय
कुमार मिश्रा की तथाकथित ‘ओरिजिनल’ स्क्रिप्ट पर फिल्म बनाने का
उनका फैसला ऐतिहासिक माना जाना चाहिए. रोहन भटनागर (हृतिक रोशन) देख
नहीं सकता, पर वो सुन सकता है, सूंघ सकता है, स्टूडियो में बिना देखे कार्टून शोज़
की परफेक्ट डबिंग कर सकता है. सुप्रिया (यामी गौतम) भी देख नहीं
सकती, पर लिपस्टिक और ऑयलाइनर इस्तेमाल करने में कभी कोई गलती नहीं करती. दोनों एक-दूसरे
से बात करते हुए बगल में रखे गमले को एकटक, बिना पलक झपकाए, चौड़ी खुली आँखें से
देखते रहते हैं, ताकि आपको उनका ‘न देख पाना’ हमेशा याद रहे. दोनों की हंसती-खेलती
जिंदगी में भूचाल तब आता है, जब एक लोकल गुंडा (रोहित रॉय) अपने बाहुबली नेता
भाई (रोनित रॉय) की शह पर सुप्रिया का बलात्कार कर देता है. भ्रष्ट सिस्टम
के सामने बेबस, लाचार रोहन के पास अपनी बीवी पर हुए अत्याचार का बदला लेने के लिए अब
सिर्फ एक ही रास्ता है, कानून अपने हाथ में ले लेना.
बलात्कार जैसा घिनौना और
ज्वलंत मुद्दा हो या ‘नेत्रहीनों’ के प्रति सही रवैया रखने-दिखाने की कवायद, ‘काबिल’
निहायत ही उदासीनता का परिचय देती है. फिल्म अपनी ओर से तनिक भी कोशिश नहीं करती कि
आप इन दोनों मुद्दों से जुड़ने का साहस दिखाएं. सब कुछ बस आपकी अपनी संवेदनशीलता पर
टिका रहता है. कहाँ तो आपको इन दोनों किरदारों के लिए ज़ज्बाती होने की सुविधा मिलनी
चाहिए थी, पर होता उल्टा है. ऐसा लगता है जैसे संजय गुप्ता की सारी
कवायद सिर्फ इस एक बात में लगी रहती है कि ‘नेत्रहीन’ भी फ़िल्मी नायक-नायिकाओं की
तरह हर वक़्त सजे-धजे हो सकते हैं. फिल्म अपने पहले हिस्से में अगर आपको किरदारों से
जोड़ने में चूक जाती है, तो भी आपको इंटरवल के बाद ये उम्मीद रहती है कि फिल्म अब
रोमांचक होने के साथ-साथ थोड़ी समझदार होने की भी हिम्मत दिखायेगी, पर धीरे-धीरे आपको
हृतिक में मिथुन की छवि दिखने लगती है, तो ये रही-सही उम्मीद भी
टूटती जाती है.
हृतिक रोशन किरदारों
में ढल जाने के लिए जाने जाते हैं, और हालाँकि फिल्म में बस वही हैं जो अपनी मौजूदगी
दर्ज कराने में अव्वल रहते हैं (रोनित रॉय ऐसे दूसरे एकलौते कलाकार हैं),
पर फिर भी एक साधारण एक्शन हीरो से ज्यादा कुछ कर गुजरने से बचते फिरते हैं. एक
अच्छी कहानी होने के बावजूद, अत्यंत सामान्य स्क्रीनप्ले के साथ उनसे इससे ज्यादा
की उम्मीद करनी भी नहीं चाहिए. मराठी कार्पोरेटर की भूमिका में रोनित न
सिर्फ भयावह लगे हैं, बल्कि एकदम सधे हुए भी. बोल-चाल हो या हाव-भाव, वो अपने
किरदार से तनिक भी अलग-थलग नहीं पड़ते. यामी गौतम खूबसूरत लगने के
अलावा कुछ और नहीं करतीं. रोहित रॉय ठीक-ठाक हैं, तो नरेन्द्र
झा और गिरीश कुलकर्णी प्रभावी.
अंत में, ‘काबिल’
हृतिक के काबिल कन्धों पर टिके होने बावजूद एक इतनी आम फिल्म है, जो न ही आपको इमोशनली
जोड़े रखने में कामयाब होती है, न ही इतनी स्मार्ट कि आप अपनी सीट से अंत तक चिपके
रहें. मिथुन दा साइकिल की आड़ में छुपकर दुश्मनों की गोलीबारी से बचते रहें?
चलता है, पर दुश्मन की थाह पाने के लिए हृतिक पूरे फ्लोर पर चिप्स और पॉपकोर्न
बिखेर कर अँधेरे में दुश्मन का इंतज़ार करें? नहीं चलता, बॉस! आप तो कोरियाई ‘रीमेक’
ही बनाओ...ओरिजिनल के नाम पर हमें बस और मत बनाओ! [2/5]